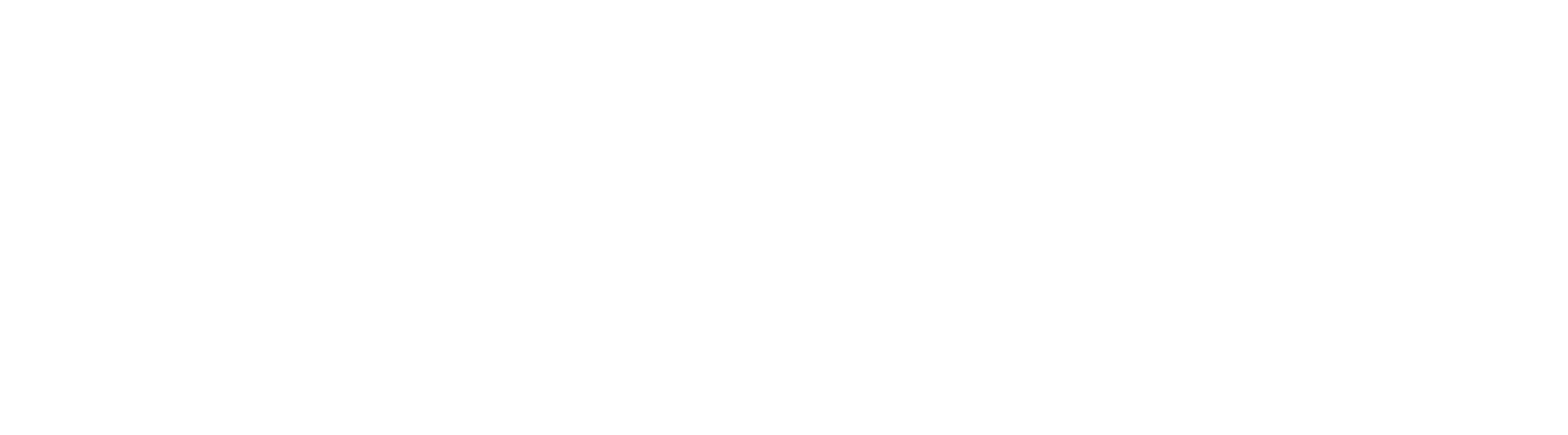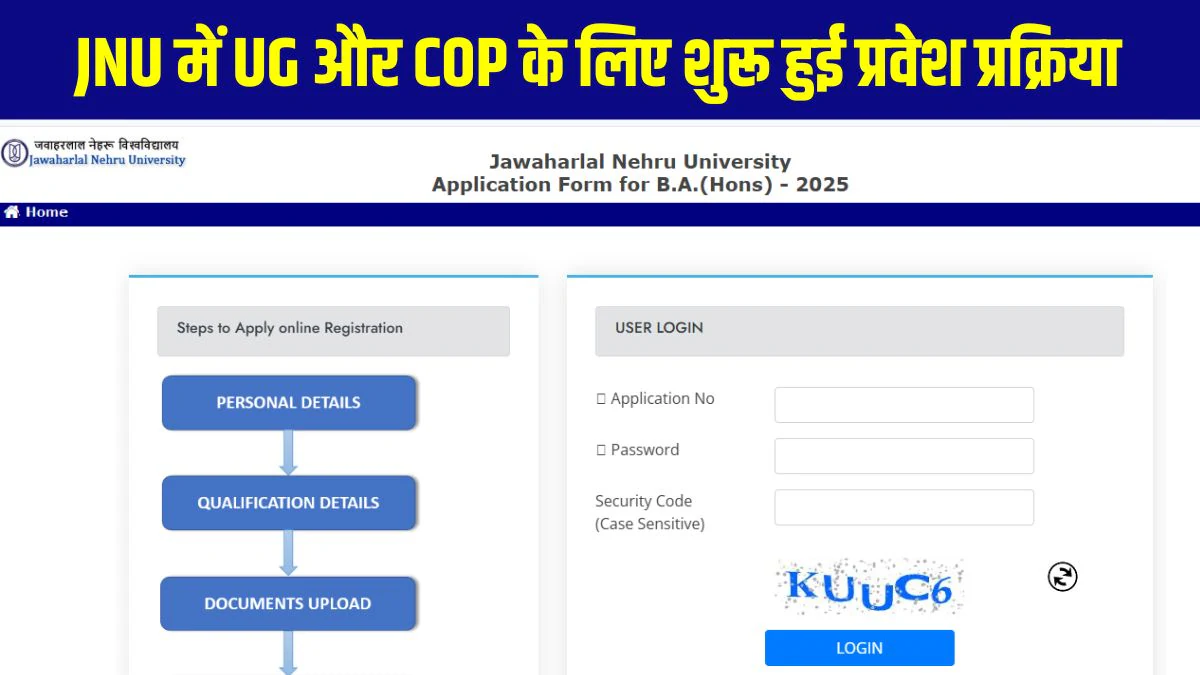परिसीमन क्या है?: भारत के चुनाव आयोग के अनुसार , परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है। यह सबसे हालिया जनगणना से संशोधित जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। परिसीमन एक संवैधानिक जनादेश है, जो निष्पक्ष और प्रतिनिधि चुनावी ढांचे और निर्वाचित निकायों में नागरिकों के न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है।
परिसीमन पर संविधान क्या कहता है?: संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या जनसंख्या के आंकड़ों से निर्धारित होती है। यह सुनिश्चित करता है कि संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले लोगों की संख्या समान रहे। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत निर्धारित एक नागरिक, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत के अनुसार है।
संविधान के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद सदनों (संसद और विधानसभा) की सीटों की संख्या को पुन: समायोजित किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 82 में कहा गया है, प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर, राज्यों को लोकसभा में सीटों का आबंटन और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करना ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे तरीके से फिर समायोजित किया जाएगा, जैसा संसद कानून के माध्यम से निर्धारित करे।
परिसीमन: क्या यूपी जैसे बड़े राज्यों के विभाजन से निपट सकता है विवाद? जानिए और क्या हो सकते हैं विकल्प
1951 में भारत की जनगणना की गई जिसके बाद 1952 के परिसीमन आयोग अधिनियम के माध्यम से पहला परिसीमन आयोग गठित किया गया। आयोग का काम लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना था। तब से इन सीमाओं को तीन बार, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियमों के तहत गठित परिसीमन आयोग द्वारा पुन: निर्धारित किया गया है ।
हाल ही में, 2001 की जनगणना के आधार पर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया गया। लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा सीटों का आबंटन और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 1972 के परिसीमन के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है।
1951 की जनगणना के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 494 तय की गई थी, जबकि 1961 की जनगणना के बाद यह संख्या 522 लोकसभा सीटों तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन 1971 के बाद से लोकसभा सीटों की संख्या 543 पर स्थिर बनी हुई है। यह संख्या लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।
आपातकाल के दौरान (25 जून 1975 – 21 मार्च 1977) प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 42वां संशोधन पारित किया, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह था कि 2000 के बाद पहली जनगणना तक 1971 की जनगणना को संदर्भ बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसने मूल रूप से 2000 के बाद की पहली जनगणना के बाद तक लोकसभा सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया।
2002 में, प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए कम से कम 2026 तक के लिए इस रोक को बढ़ा दिया। लोकसभा सीटों की संख्या पर यही रोक है, जिसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन केंद्र से 30 वर्षों के लिए बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं।
सबसे पहले राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग की नियुक्ति करते हैं । इस आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके प्रतिनिधि और राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल होते हैं।
इसके अलावा, प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सहयोगी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जहां परिसीमन होना है। ये सदस्य आम तौर पर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त संसद सदस्य और प्रत्येक विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त विधानसभा के सदस्य होते हैं। आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसकी तैयार की गई संशोधित सीमाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती।
एक बार जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो परिसीमन आयोग अपनी सिफारिशें आम करता है और आम जनता, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों की प्रतिक्रिया आमंत्रित करता है। आधिकारिक राजपत्र में छपने के बाद, आयोग के आदेश अगले चुनाव में प्रभावी होते हैं।