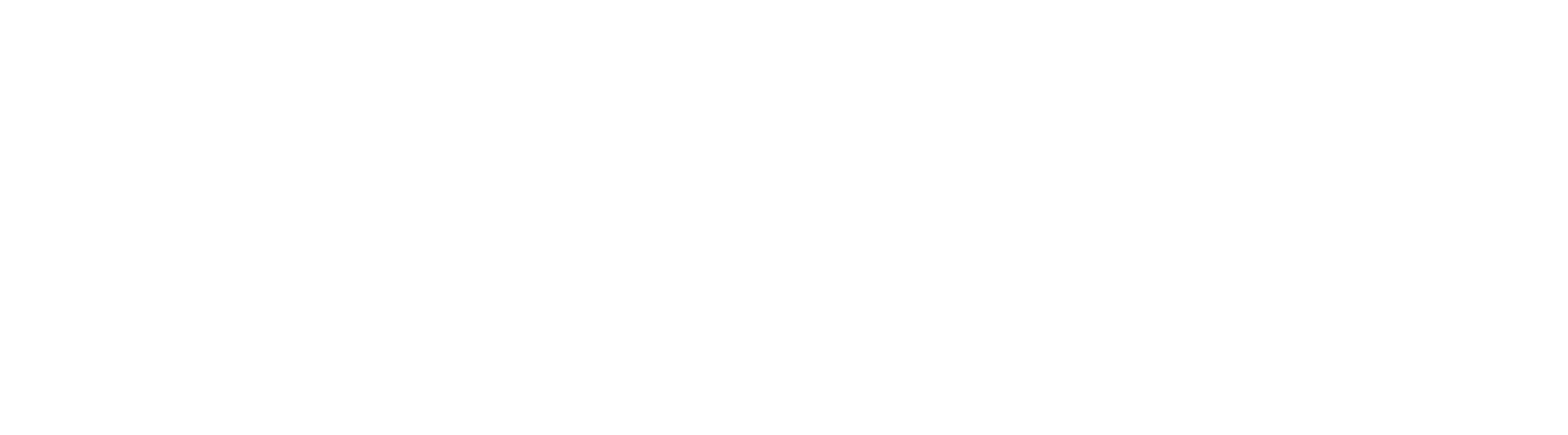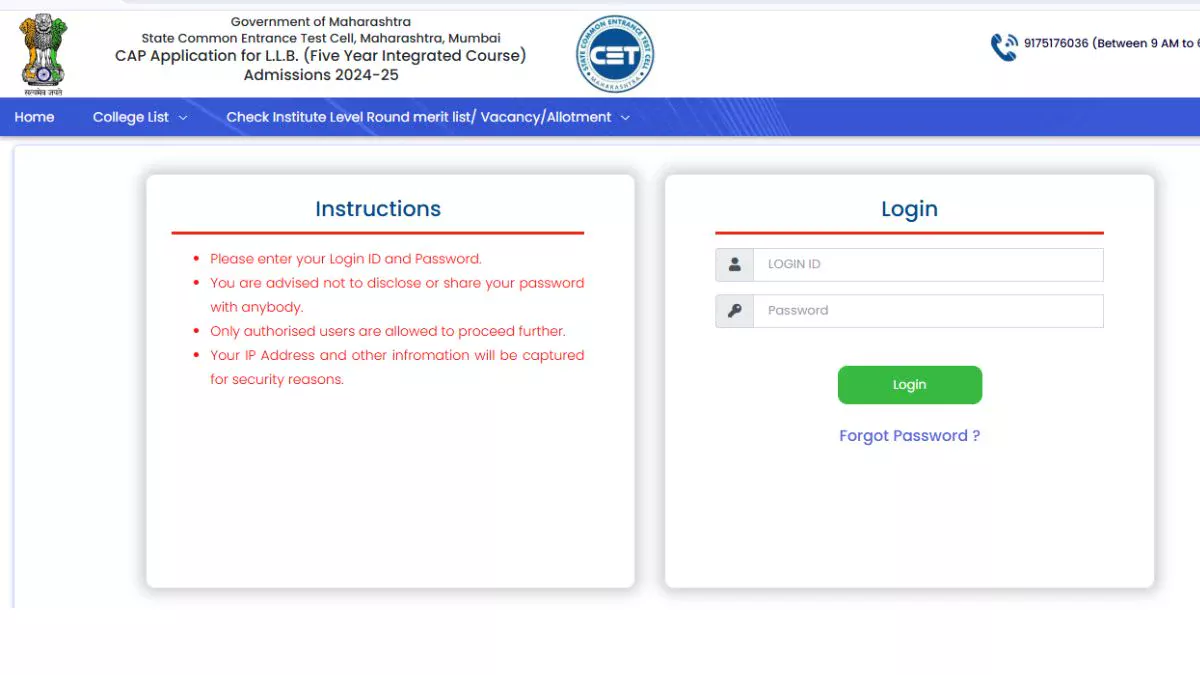Delimitation Debate: परिसीमन पर बहस साल 2026 में काफी तेज होने वाली है। लगभग सभी विपक्षी पार्टियां इस बात पर सहमत है कि जनसंख्या को लोकसभा सीटों के रिओपोरशन का एकमात्र आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा इस वजह से इससे उन राज्यों को सजा दी जाएगी जो अपनी जनसंख्या बढ़ोतरी को कम करने में कामयाब रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कई ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें परिसीमन को प्रजनन दर से जोड़ने से लेकर राज्यसभा में सुधार तक शामिल है।
सबसे आसान हल यह है कि लोकसभा में सीटों की संख्या को संवैधानिक सीमा 550 से ऊपर बढ़ाया जाए, ताकि हर एक सीट जनसंख्या के संदर्भ में पूरे देश में समानता की जा सके। अमेरिका स्थित थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के फेलो मिलन वैष्णव और जेमी हिंटसन के अनुसार, 2026 के लिए अनुमानित जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा को 848 निर्वाचन क्षेत्रों की जरूरत होगी ताकि यह तय किया जा सके रिओपोरशन से किसी भी राज्य की मौजूदा सीटें कम न हों। लोकसभा सीटों की सीमा बढ़ाने का एक फायदा यह है कि इससे प्रति सीट जनसंख्या कम रखने में मदद मिलेगी। इसको एक उदाहरण के जरिये समझने की कोशिश करें तो 848 सीटों वाले विधान सभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को 143 सीटें मिलेंगी। यह इस समय 80 हैं और तमिलनाडु को 49 सीटें मिलेंगी। यह इस वक्त 39 हैं।
रंगराजन आर ने एक रिपोर्ट में तर्क दिया कि भारत की जनसंख्या चरम पर पहुंच जाएगी और 2060 के दशक में घटने लगेगी। उन्होंने कहा कि इसके बजाय, राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ कहीं ज्यादा पास से काम करते हैं। इस समय परिसीमन के ढांचे में हर एक सीट का मतलब कुल आबादी का प्रतिनिधित्व करना है, चाहे वह मतदान करने की उम्र के हों या नहीं या किसी स्पेशल निर्वाचन क्षेत्र के वोटर के तौर पर रजिस्टर हो या नहीं। कई राज्यों में लोग उन निर्वाचन क्षेत्रों के मूल निवासी नहीं हो सकते हैं जहां वे रहते हैं, लेकिन फिर भी परिसीमन सूत्र में उनकी गिनती होती है।
क्या है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया?
इस को दूर करने के लिए सिर्फ वोटर की संख्या के आधार पर सीटों पर बंटवारा करने का तर्क दिया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी प्रणाली चुनावों में प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए काम करने वाले या वास्तव में काम करने वाले लोगों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का आकार तय करने के लिए ज्यादा वैलिड हो सकती है। हालांकि, इस रिपोर्ट में डिग्रेसिव प्रोपोरशनिली मेथड का भी सुझाव दिया गया है। इसके तहत ज्यादा आबादी वाले राज्य कम प्रतिनिधित्व के लिए सहमत होते हैं, ताकि कम आबादी वाले राज्यों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके।
उदाहरण के लिए कनाडा ने 2011 में अपने संविधान में संशोधन करके बड़े, तेजी से बढ़ते प्रांतों और छोटे, कम स्पीड से बढ़ते प्रांतों के बीच संतुलन बनाने के लिए डिग्रेसिव प्रोपोर्शनल लागू किया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपे एक पेपर में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस राजा सेतु दुरई और तमिलनाडु राज्य योजना आयोग के सदस्य आर श्रीनिवासन ने पाया कि कनाडाई प्रणाली को लोकसभा में लागू करने से इसकी कुल संख्या 552 हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जबकि उत्तर प्रदेश को ज्यादा नौ सीटें मिलेंगी, जिससे यह 89 हो जाएगी। वहीं तमिलनाडु की सीटें 39 ही रहेंगी।
दुरई और श्रीनिवासन की तरफ से यह तर्क दिया गया कि टोटल फर्टिलिटी रेट को भी परिसीमन में शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या के खिलाफ संतुलन के लिए टीएफआर का इस्तेमाल किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीएफआर को कंट्रोल करने वाले राज्यों को दंडित न किया जाए। इस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए दुरई और श्रीनिवासन ने 2011 की जनगणना से टीएफआर-समायोजित आबादी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया।
उनकी कैलकुलेशन से पता चलता है कि लोकसभा की संख्या को 750 तक बढ़ाना होगा, लेकिन सीटों का इस तरह से रिओपोरशन किया जा सकता है कि कम स्पीड से बढ़ती आबादी वाले राज्यों को नुकसान ना पहुंचे। उदाहरण के लिए, जबकि उत्तर प्रदेश को 106 सीटें मिलेंगी और बिहार को 50 सीटें वर्तमान में 40 मिलेंगी, तमिलनाडु जैसे कम आबादी वाले राज्य को 55 सीटें मिलेंगी।
परिसीमन को लेकर तमिलनाडु से पंजाब तक क्यों बढ़ रही चिंता
लोकसभा सीटों के परिसीमन के नेगेटिव इफेक्ट्स को बैलेंस करने के लिए राज्यसभा में सुधार की भी वकालत की गई है। विधि सेंटर की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा प्रावधानों के तहत राज्यसभा में सीटें डिग्रेसिव प्रोपोरशनिली के आधार पर आवंटित की जाती हैं, जो छोटे राज्यों की डिवेल्यू नहीं करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फॉर्मूले के तहत राज्यों को पहले पांच मिलियन तक हर दस लाख लोगों पर एक सीट दी जाती है।
हालांकि, समय के साथ इस फॉर्मूले को तर्कसंगत नहीं बनाया गया है। इस समय 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में राज्यसभा की 250 सीटों में से 156 सीटें हैं और नौ सबसे कम आबादी वाले राज्यों में से हर एक के पास एक-एक सीट है। यूरोपीय संसद का उदाहरण देते हुए, विधि केंद्र ने हर एक राज्य के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीटों की संख्या तय करने और सीटों को इस तरह से आवंटित करने का सुझाव दिया है जिससे छोटे राज्यों को वंचित न किया जाए। राज्यसभा के पास में कुछ सीमित ही शक्तियां हैं।
इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव दिया गया कि राज्य सभा एक निर्वाचित निकाय हो, अमेरिकी सीनेट की तरह जिसमें हर राज्य से दो सदस्य होते हैं, ताकि लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का संतुलन बनाया जा सके। हालांकि, एक निर्वाचित राज्य सभा, चाहे सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई हों या हर एक राज्य को समान संख्या में सीटें दी गई हों, तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि राज्यसभा धन विधेयकों में संशोधन नहीं कर सकता और अधिवास की जरूरत को बहाल नहीं किया जाता।