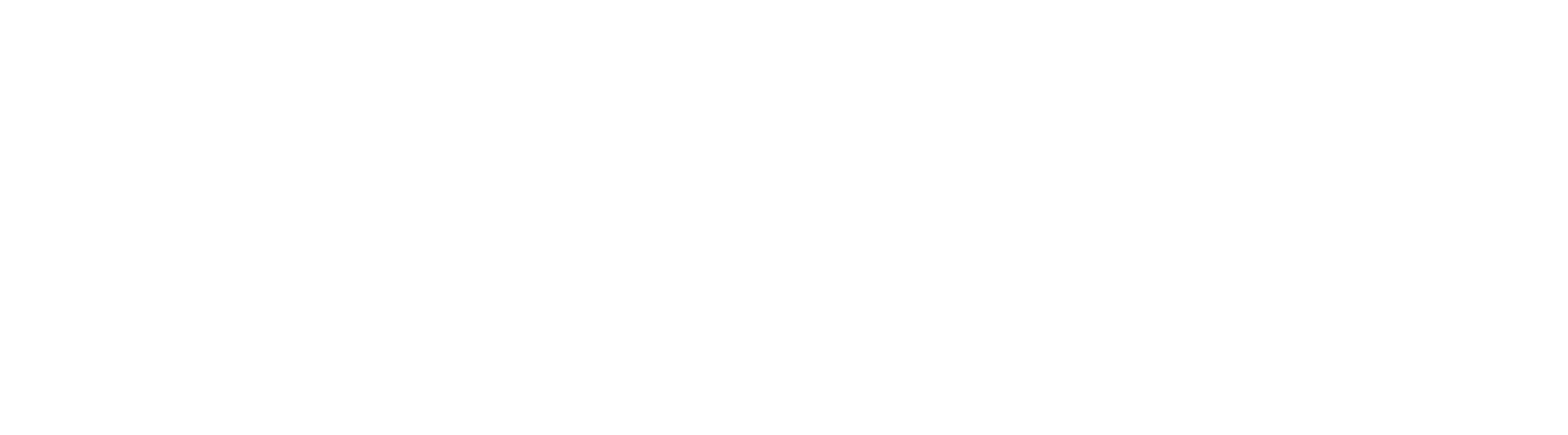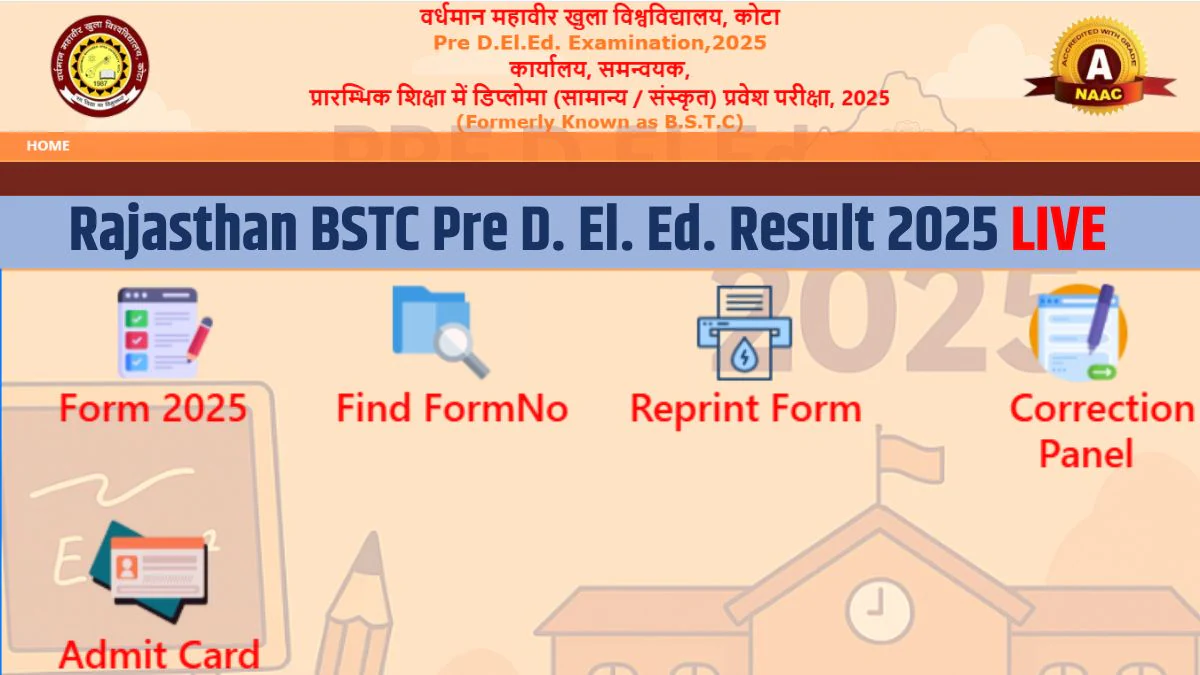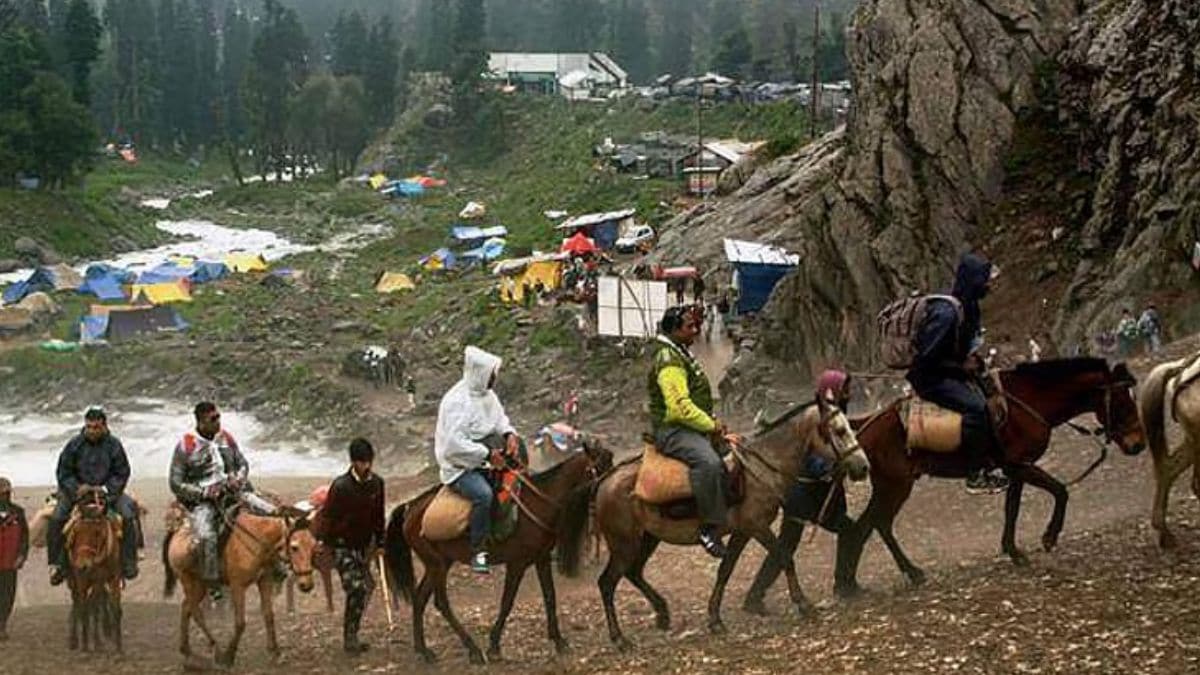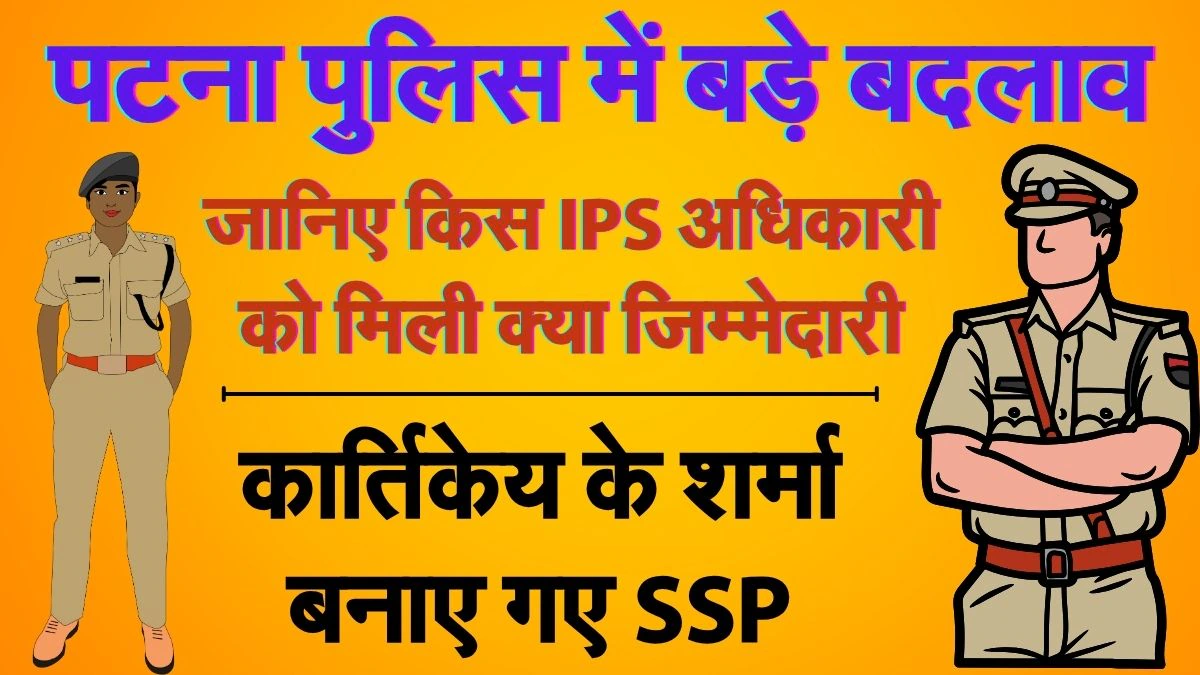(इंडियन एक्सप्रेस ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इतिहास, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, कला, संस्कृति और विरासत, पर्यावरण, भूगोल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि से जुड़े मुद्दों और अवधारणाओं पर अनुभवी लेखकों एवं विद्वानों द्वारा लिखे गए लेखों की एक नई श्रृंखला शुरू की है। विषय विशेषज्ञों के साथ पढ़ें, विचार करें और बहुप्रतीक्षित यूपीएससी सीएसई पास करने के अपने अवसर को बढ़ाएं। निम्नलिखित लेख में पौराणिक कथाओं एवं संस्कृति के विशेषज्ञ, प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक बताते हैं कि संस्कृति को समझने के लिए बर्तन कैसे आवश्यक हैं।)
मिट्टी के बर्तन संस्कृति के प्रतीक हैं। उन्होंने मनुष्यों को भोजन और पानी के परिवहन की अनुमति दी। खाना पकाने या भंडारण के अलावा, वे विवाह और मृत्यु समारोहों में अनुष्ठानिक उद्देश्यों की भी पूर्ति करते हैं। यह दोहरा कार्य – व्यावहारिक और आध्यात्मिक – मिट्टी के बर्तनों को सांस्कृतिक विरासत का एक अनिवार्य पहलू बनाता है।
भारत अपने लोटे के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य पूर्व की सुराही और ग्रीक एम्फ़ोरा से भिन्न है। लोटे के मुंह पर एक किनारा, एक गर्दन और एक गोलाकार शरीर होता है, जो कमल की कली जैसा दिखता है। यह सुराही से अलग है, जिसमें किनारा नहीं होता, गर्दन लंबी होती है और इसका आकार रैखिक होता है, जो लिली की कली के समान प्रतीत होता है। लोटे का आधार आमतौर पर गोल होता है, जिससे इसे नरम मिट्टी या सपाट सतह पर आसानी से रखा जा सकता है।
सुराही का आधार अक्सर नुकीला और शंक्वाकार होता है, जिससे इसे जहाज पर लकड़ी के तख्तों के बीच रखने या रेत में दबाकर सीधा खड़ा करने में सुविधा होती है। लोटा और सुराही के किनारे पर एक थूथन हो सकता है, जबकि एम्फ़ोरा में दोनों तरफ़ दो हैंडल होते हैं। हालांकि, लोटे को हैंडल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसे गर्दन से आसानी से पकड़ा जा सकता है।
भारत में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग केवल पानी या दूध रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। बर्तनों का उपयोग देवताओं के प्रतीक के रूप में और अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किया जाता रहा है। इन्हें अक्सर नारियल, केले, आम के पत्ते और फूल जैसी पवित्र वस्तुओं से भरा जाता है।
आज भी धार्मिक समारोहों और मंदिर अनुष्ठानों के दौरान शुभता और दिव्यता की उपस्थिति का प्रतीक करने के लिए बर्तन रखे जाते हैं। यह प्रथा हज़ारों साल पुरानी है। कश्मीरी पंडित अनुष्ठानों में शिव, शक्ति और भैरव का प्रतिनिधित्व करने के लिए संकीर्ण मुंह वाले बड़े बर्तनों का उपयोग करते हैं, जिनमें देवताओं को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद भरा जाता है।
बौद्ध स्तूपों और मंदिरों में पूर्ण कुंभ भी पाया जाता है, जो उर्वरता और जीवन से भरपूर एक बर्तन है। इसमें से पौधे, फूल और फल फूटते हुए दर्शाए जाते हैं, जो बहुतायत का प्रतीक हैं—यह हॉर्न ऑफ़ प्लेंटी या अक्षय पात्र की अवधारणा के समान है। अमृत कुंभ, या अमृत का बर्तन, भारतीय संस्कृति में एक और महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है।
हिंदू परंपराओं में मिट्टी के बर्तन मृत्यु संस्कारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतिम संस्कार की चिता जलाने के लिए रसोई से आग एक बर्तन में लाई जाती है। हिंदू अंतिम संस्कार समारोह के दौरान, चिता को अग्नि देने से पहले पानी से भरे बर्तन को तोड़ा जाता है। मृतक की हड्डियों और राख को एक बर्तन में एकत्र कर घर के बाहर लटकाया जाता है, जब तक कि उन्हें नदी में विसर्जित करने का समय न आ जाए। प्रारंभिक वैदिक काल में, इन हड्डियों से भरे बर्तनों को सीधे जमीन में दफना दिया जाता था।
प्रागैतिहासिक काल में, बर्तनों का उपयोग दफनाने की रस्मों में भी किया जाता था। महाराष्ट्र के इनामगांव में, मेगालिथिक काल (लौह युग, लगभग 1000 ईसा पूर्व) का एक बर्तन मिला था जिसमें एक मानव कंकाल था। तमिल संगम कविता में, एक विधवा कुम्हार से अपने मृत पति के लिए पर्याप्त बड़ा बर्तन बनाने के लिए कहती है।
भारत में सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन हड़प्पा सभ्यता के हैं। प्रागैतिहासिक मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, क्योंकि कुम्हार का चाक बाद में आया था। ये शुरुआती बर्तन अक्सर लाल रंग के होते थे जिन पर मोर, भैंस, पीपल के पेड़, नीम के पेड़ और ज्यामितीय पैटर्न जैसे कि प्रतिच्छेदन रेखाएँ और वृत्त काले रंग से पेंट किए गए थे।
कुछ विद्वानों का तर्क है कि दक्षिण भारत में पाए गए लाल और काले रंग के बर्तन हड़प्पा क्षेत्र (3500 साल पहले) से तमिल क्षेत्र (2000 साल पहले) में लोगों के संभावित प्रवास का संकेत देते हैं।
मिट्टी के बर्तनों की शैलियों में एक बड़ा बदलाव वैदिक काल (लगभग 1000 ईसा पूर्व – 500 ईसा पूर्व) के दौरान हुआ। इस युग में चित्रित ग्रे बर्तनों का उदय हुआ – काली रेखाओं से सजे ग्रे बर्तन। ये बर्तन गंगा के क्षेत्र में महाभारत और रामायण की घटनाओं से जुड़े स्थानों पर पाए गए हैं।
बाद में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय और महाजनपद काल के दौरान शहरी केंद्रों के उद्भव के बाद, मिट्टी के बर्तनों का एक और विशिष्ट प्रकार उभरा – उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन। यह बढ़िया काले मिट्टी के बर्तन (500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व) बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों और व्यापार से जुड़े थे।
मिट्टी के बर्तनों में अगला महत्वपूर्ण विकास ग्लेज्ड पोर्सिलेन के साथ हुआ, जो चीन से लगभग 1000 ईस्वी में भारत आया। चीन के साथ व्यापार भूमि और समुद्री दोनों मार्गों से फैला। भूमि मार्ग मध्य एशिया, फारस और तुर्की से होकर गुजरता था, जबकि समुद्री मार्ग वियतनाम और इंडोनेशिया के माध्यम से दक्षिणी चीन को भारत के तटीय क्षेत्रों से जोड़ता था। जब मुस्लिम व्यापारी भारत आए, तो वे चमकीले चीनी मिट्टी के बर्तन लाए, जिन्हें आमतौर पर “चीनी बर्तन” कहा जाता है।
(देवदत्त पटनायक एक प्रसिद्ध पौराणिक कथाकार हैं जो कला, संस्कृति और विरासत पर लिखते हैं।)